Read more
ऊष्मा और ऊष्मागतिकी(Heat and Thermodynamics)
ऊष्मा और ऊष्मागतिकी (Heat and Thermodynamics) – NCERT आधारित संक्षिप्त सारांश
1. परिचय
ऊष्मा और ऊष्मागतिकी भौतिकी व रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊष्मा (Heat), कार्य (Work), ऊर्जा (Energy) और उनके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम सभी प्रकार की भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में लागू होते हैं—जैसे इंजन, रेफ्रिजरेटर, मानव शरीर, प्राकृतिक घटनाएँ आदि।
2. मुख्य अवधारणाएँ
-
ऊष्मा (Heat): वह ऊर्जा, जो तापांतर के कारण एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित होती है।
-
ताप (Temperature): किसी वस्तु के ऊष्मीय स्तर का माप।
-
आंतरिक ऊर्जा (Internal Energy): किसी सिस्टम के अणुओं की कुल गतिज एवँ स्थितिज ऊर्जा।
3. ऊष्मागतिकी के प्रमुख नियम (Laws of Thermodynamics)
(a) शून्यवाँ नियम (Zeroth Law)
-
यदि दो Systems, किसी तीसरे System के साथ ऊष्मीय संतुलन (Thermal Equilibrium) में हैं, तो वे आपस में भी संतुलन में हैं।
-
इससे “तापमान (Temperature)” की परिभाषा संभव होती है।
(b) ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम (First Law)
-
ऊर्जा संरक्षण का नियम: ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, न नष्ट – केवल एक रूप से दूसरे में बदल सकती है।
-
गणितीय रूप में:
जहाँ
= आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन,
= सिस्टम को दी गई ऊष्मा,
= सिस्टम द्वारा किया गया कार्य।
(c) ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम (Second Law)
-
ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर स्वप्रेरणा से प्रवाहित होती है।
-
एंट्रॉपी (Entropy): प्रत्येक स्वाभाविक प्रक्रिया में संपूर्ण एंट्रॉपी बढ़ती है या यथावत रहती है।
-
क्लॉज़ियस कथन: ऊष्मा कभी भी शीतल बिंदु से उष्ण बिंदु की ओर स्वाभाविक रूप से नहीं जा सकती।
-
केल्विन–प्लैंक कथन: ऐसी कोई प्रक्रिया संभव नहीं है जिसमें सम्पूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सके।
4. मुख्य ऊष्मागतिकीय प्रक्रियाएँ
| प्रक्रिया | विशेषता | उदाहरण |
|---|---|---|
| समतापी (Isothermal) | तापमान स्थिर () | बर्फ पिघलना |
| रुद्धोष्म (Adiabatic) | ऊष्मा आदान-प्रदान नहीं () | त्वरित गैस का संपीड़न |
| समदाब (Isobaric) | दाब स्थिर () | पानी का उबलना खुले बर्तन में |
| समायतनिक (Isochoric) | आयतन स्थिर () | ऑटोक्लेव में गैस गर्म करना |
-
ऊष्मा इंजन: वह यंत्र जो ऊष्मा को कार्य में बदलता है (जैसे—भाप इंजन)।
-
कार्नोट इंजन: आदर्श इंजन; इसकी कार्य क्षमता (Efficiency) सर्वाधिक होती है।
-
दक्षता (Efficiency):
जहाँ = उच्च तापीय स्रोत का तापमान, = निम्न तापीय सिंक का तापमान (केल्विन में)।
6. महत्वपूर्ण सूत्र
| विषय | सूत्र |
|---|---|
| आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन | |
| कार्य (गैस विस्तार/संपीड़न) | |
| दक्षता (कार्नोट इंजन) | |
| एंट्रॉपी परिवर्तन |
-
थर्मोडायनामिक्स के नियम मशीनों, रेफ्रिजरेटर, एसी, पावरहाउस, जैविक प्रक्रमों व रासायनिक प्रतिक्रियाओं की आधारशिला हैं।
-
इंजीनियरिंग, पर्यावरण, औद्योगिक प्रक्रियाओं, तथा रोजमर्रा के जीवन में इनका उपयोग व्यापक है।
8. संक्षिप्त निष्कर्ष
-
ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांतों को समझाते हैं।
-
संपूर्ण प्राकृतिक घटनाएँ ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करती हैं।
-
परीक्षाओं व व्यवहारिक जीवन में यह अध्याय अत्यंत उपयोगी व आधारभूत है।
ऊष्मा (Heat) – NCERT आधारित संक्षिप्त सारांश (हिन्दी में)
1. परिचय
-
ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, जो किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा बनाती है।
-
ऊष्मा हमेशा तापमान में अंतर वाले दो निकायों या वस्तुओं के बीच, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है।
-
इससे चीज़ों के तापमान में परिवर्तन आता है और यह ऊर्जा का संचारण है।
2. ऊष्मा और ताप (Heat and Temperature)
-
ऊष्मा: एक प्रकार की ऊर्जा, जिसका मात्रक “कैलोरी” (Calorie) या “जूल” (Joule) है।
-
ताप: किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का माप, जिसे “डिग्री सेल्सियस” (°C) या “केल्विन” (K) में मापा जाता है।
-
तापमापी (Thermometer) द्वारा ताप मापा जाता है—स्पर्श केवल अनुमान बता सकता है, सही माप नहीं।
3. ऊष्मा का स्थानांतरण (Transfer of Heat)
ऊष्मा के संचरण की तीन प्रमुख विधियाँ हैं:
-
चालन (Conduction):
-
ठोस पदार्थों में ऊष्मा उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग में अपने संपर्क के द्वारा।
उदाहरण: धातु की छड़ के एक सिरे को गरम करने पर दूसरा सिरा भी गरम हो जाता है।
-
-
संवहन (Convection):
-
द्रवों (Liquid) और गैसों में ऊष्मा का संचरण कणों के गति के कारण होता है।
उदाहरण: पानी गर्म करना—नीचे के कण गरम होकर ऊपर, ऊपर के ठंडे कण नीचे आते हैं।
-
-
विकिरण (Radiation):
-
जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम के तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसे विकिरण कहते हैं।
उदाहरण: सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आना।
-
4. मुख्य अवधारणाएँ और तथ्य
-
गर्म वस्तु से ऊष्मा बाहर जाती है, ठंडी वस्तु में जाती है।
-
दो वस्तुओं का ताप समान होने पर, उनके बीच ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता।
-
ऊष्मा प्राप्त करने या छोड़ने से वस्तु के ताप में वृद्धि या कमी आती है।
-
किसी पदार्थ की ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा—पदार्थ के द्रव्यमान, तापांतर तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा (Specific Heat) पर निर्भर करती है।
-
विशिष्ट ऊष्मा: किसी पदार्थ के एक ग्राम (या १ किलोग्राम) का ताप १°C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा।
-
गुप्त ऊष्मा: जब पदार्थ अवस्था बदलता है, जैसे बर्फ से पानी में या पानी से भाप में—अतिरिक्त ऊष्मा ताप में वृद्धि किए बिना ही खर्च हो जाती है।
5. अन्य रोचक बातें व अनुप्रयोग
-
कपड़ों की कई परतें या वायु ऊष्मा के अच्छे रोधक (Insulator) होते हैं, जिससे गर्मी बचाए रखी जा सकती है।
-
धातुएँ ऊष्मा की अच्छी चालक (Conductors), जबकि लकड़ी, वायु आदि ऊष्मा की रोधक (Insulators) हैं।
-
अधिकांश ऊष्मा अवधारणाएँ दैनंदिन जीवन—खाना पकाना, हीटर, कुकर, घरों की बनावट आदि में लागू होती हैं।
ताप (Temperature) – NCERT आधारित संक्षिप्त सारांश
1. परिभाषा
-
ताप किसी वस्तु की गरमाहट या ठंडक का मात्रक माप है।
-
अर्थात, ताप यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है।
-
जब दो वस्तुएँ संपर्क में आती हैं, तो ऊष्मा उच्च ताप वाली से निम्न ताप वाली की ओर प्रवाहित होती है—इससे उनके ताप को आपस में तुलना की जा सकती है।
2. ताप और ऊष्मा का अंतर
-
ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, जबकि ताप उसकी स्थिति (thermal state) का माप है।
-
ऊष्मा, तापांतर के कारण प्रवाहित होती है, लेकिन ताप स्वयं ऊर्जा नहीं है, यह ऊर्जा का माप है।
3. ताप का मापन
-
तापमापी (Thermometer) वह यंत्र है, जिससे ताप मापा जाता है।
-
डॉक्टरी तापमापी: शरीर का ताप मापना (सामान्य सीमा—35°C से 42°C)
-
प्रयोगशाला तापमापी: पदार्थों का ताप मापना (सीमा –10°C से 110°C)।
-
-
मानव शरीर का सामान्य ताप: 37°C या 98.6°F
4. ताप के मात्रक और मापक्रम
-
तीन प्रमुख ताप मापक्रम:
-
डिग्री सेल्सियस (°C)
-
डिग्री फारेनहाइट (°F)
-
केल्विन (K) – SI मात्रक
-
-
रूपांतरण सूत्र:
-
°F = × °C + 32
-
K = °C + 273.15
-
5. अन्य तथ्य
-
केवल स्पर्श से सही–सही ताप का पता नहीं चलता, इसलिए उपकरणों (थर्मामीटर) से मापन किया जाता है।
-
एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप सामान्यतः 37°C होता है।
-
तापमापी की सटीकता के लिए उसमें प्रयुक्त द्रव्य (जैसे–पारा या अन्य डिजिटल सेंसर) ताप परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं।
6. सारांश तालिका
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| ताप क्या है? | किसी वस्तु की गरमाहट/ठंडक का माप |
| SI मात्रक | केल्विन (K) |
| शरीर का सामान्य ताप | 37°C या 98.6°F |
| तापमापी के प्रकार | डॉक्टरी व प्रयोगशाला तापमापी |
| मापक्रम | डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन |
ताप के सही मापन हेतु थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए, न कि केवल स्पर्श के अनुभव से तय करना चाहिए।
ताप के अध्ययन से दैनिक जीवन, विज्ञान और स्वास्थ्य–सुरक्षा में सही कदम उठाए जा सकते हैं
आंतरिक ऊर्जा (Internal Energy) – NCERT आधारित संक्षिप्त सारांश
1. परिभाषा
-
आंतरिक ऊर्जा (Internal Energy) किसी तंत्र (System) में निहित कुल ऊर्जा को कहते हैं।
-
इसमें उस तंत्र के सभी कणों की गतिज ऊर्जा (Molecular Kinetic Energy) और स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy) दोनों शामिल होती हैं, जैसे—घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि।
-
इसे प्रायः या से दर्शाया जाता है।
2. मुख्य बिंदु
-
कार्यात्मक परिभाषा:
आंतरिक ऊर्जा तंत्र की अवस्था (Temperature, Pressure, Volume एवं Composition) पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे अवस्था जात गुण (State Function) कहते हैं। -
इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना असंभव है—केवल दो अवस्थाओं में आए परिवर्तन () ही ज्ञात किए जा सकते हैं।
-
ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार—ऊष्मा या कार्य करने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बदलती है:
जहाँ = तंत्र में दी गई ऊष्मा, = तंत्र द्वारा किया गया कार्य।
3. आंतरिक ऊर्जा के घटक (Components):
-
गतिज ऊर्जा () — कणों की गति (अनुवाद, कंपन, घूर्णन)
-
स्थितिज ऊर्जा () — कणों के बीच आकर्षण-प्रतिरोध, परमाण्विक/इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा
इस प्रकार
संकलित रूप में:
(इलेक्ट्रॉनिक, नाभिकीय, अनुवाद, घूर्णन, कंपन एवं अन्य)।
4. आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन (Change in Internal Energy):
-
किसी तंत्र पर ऊष्मा देने या कार्य करने से उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ सकती है या घट सकती है।
-
केवल परिवर्तन () ही मायने रखता है:
-
यदि तंत्र ऊष्मा प्राप्त करता है, , तो बढ़ेगी।
-
यदि तंत्र कार्य करता है, , तो घटती है।
-
5. महत्व एवं अनुप्रयोग
-
ऊष्मागतिकी, रासायनिक अभिक्रियाएँ, इंजन, जीव विज्ञान के ऊष्मा-ऊर्जा विनिमय आदि—सभी में आंतरिक ऊर्जा विश्लेषण ज़रूरी है
-
आदर्श गैसों के लिए,
( = मोल संख्या, = विशिष्ट उच्च ताप पर ऊष्मा, = ताप)।
6. सारांश तालिका
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| परिभाषा | तंत्र में निहित कुल ऊर्जा |
| SI मात्रक | जूल (Joule) |
| घटक | गतिज + स्थितिज ऊर्जा |
| निरपेक्ष मान | ज्ञात नहीं, केवल परिवर्तन ज्ञात |
| सूत्र | (ऊष्मागतिकी प्रथम नियम) |
आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और ताप जैसे अध्यायों को सीखने तथा ऊष्मागतिकी के नियमों को समझने की आधारशिला है। इसकी गहरी समझ प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं दोनों में अत्यंत लाभदायक है।
ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम (Zeroth Law of Thermodynamics) – NCERT आधारित संक्षिप्त सारांश
1. परिभाषा एवं सारांश
-
शून्यवाँ नियम कहता है कि यदि दो प्रणालियाँ (Systems) किसी तीसरी प्रणाली के साथ तापीय साम्यावस्था (Thermal Equilibrium) में होती हैं, तो वे आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होंगी.
-
सरल शब्दों में: अगर System A और System B दोनों System C के साथ तापीय साम्यावस्था में हैं, तो A और B भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे।
-
यही नियम तापमान (Temperature) की अवधारणा को परिभाषित और स्थापित करता है।
2. महत्वपूर्ण बिंदु
-
तापीय साम्यावस्था (Thermal Equilibrium): जब दो निकायों का ताप (Temperature) बराबर हो जाता है और उनके बीच ऊष्मा (Heat) का प्रवाह बंद हो जाता है।
-
मापनीय ताप: शून्यवाँ नियम ही ताप व्यावहारिक रूप से मापने की आधारशिला देता है। इसी कारण थर्मामीटर (Thermometer) को अन्य किसी जिस्म का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
-
नियम का महत्व: तापमान की तुलना तथा विज्ञान और इंजीनियरिंग की सभी ऊष्मागतिकी अवधारणाओं की शुरुआत इसी नियम से होती है।
3. सरल उदाहरण
-
यदि थर्मामीटर और पानी एक ही तापमान पर है, और थर्मामीटर और दूध भी उसी तापमान पर हैं, तो दूध और पानी भी आपस में एक ही तापमान पर होंगे।
4. सारणीबद्ध जानकारी
| विषय | सारांश |
|---|---|
| नाम | ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम |
| मुख्य बात | यदि दो प्रणालियाँ तीसरी के साथ तापीय साम्यावस्था में हैं, तो वे आपस में भी साम्यावस्था में होंगी |
| महत्व | तापमान की अवधारणा और मापन की आधारशिला |
| उदाहरण | थर्मामीटर, पानी और दूध |
-
शून्यवाँ नियम ताप और तापमान की बुनियादी समझ को मजबूत करता है और ऊष्मा-ऊर्जा प्रयोगों की व्यवहारिक शुरुआत इसी नियम से होती है.
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम (First Law of Thermodynamics) – NCERT आधारित संक्षिप्त सारांश
1. परिभाषा
-
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जिसके अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट—इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
-
ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा के बीच संबंध को दर्शाता है—जब एक तंत्र ऊष्मा प्राप्त करता है या उस पर कार्य होता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
2. गणितीय अभिव्यक्ति
-
प्रथम नियम को गणितीय रूप से इस प्रकार लिखा जाता है:
या कई उच्चतर पुस्तकों में,
जहाँ,
-
= तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन,
-
= तंत्र में दी गई ऊष्मा (सकारात्मक जब तंत्र ऊष्मा प्राप्त करता है),
-
= तंत्र द्वारा किया गया कार्य (सकारात्मक जब तंत्र पर कार्य किया जाता है)।
-
3. मुख्य बातें और उदाहरण
-
जब किसी तंत्र में ऊष्मा दी जाती है और वह तंत्र वर्क करता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में के अनुसार परिवर्तन होगा।
-
यदि तंत्र इन्सुलेटेड (अलग-थलग) है तो कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी।
-
उदाहरण: भाप इंजन, रेफ्रिजरेटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, गैस संपीड़न या विस्तार आदि प्रक्रियाओं में यह नियम लागू होता है।
-
ऊष्मा प्राप्त करने पर या तंत्र पर कार्य करने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है; कार्य करने पर या ऊष्मा खोने पर घटती है।
4. प्रभाव व उपयोगिता
-
प्रथम नियम के कारण ऊर्जा की गणना, यंत्र/इंजन की दक्षता, जैविक प्रक्रमों और रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा-व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है।
-
यह सभी ऊष्मागतिकी प्रतिक्रियाओं की आधारशिला है।
5. सारणी:
| विषय | सूत्र/बिंदु |
|---|---|
| ऊर्जा संरक्षण | ऊर्जा न नष्ट, न उत्पन्न – केवल रूपांतरण |
| गणितीय रूप | या |
| मुख्य घटक | आंतरिक ऊर्जा (), ऊष्मा (), कार्य () |
| महत्व | ऊष्मागतिकी प्रक्रियाओं का आधार |
प्रथम नियम के अनुसार तंत्र की कुल ऊर्जा का परिमाण – ऊष्मा और कार्य के जोड़/घटाव रूप में बदलता है।
यह नियम पदार्थ की सभी अवस्थाओं (ठोस, द्रव, गैस) एवं सभी ऊष्मागतिक प्रसंगों पर लागू होता है।
ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम (Second Law of Thermodynamics) – NCERT आधारित संक्षिप्त सारांश
1. परिचय
-
ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्राकृतिक ऊष्मीय प्रक्रियाओं की दिशा और सीमा निर्धारित करता है।
-
यह बताता है कि गर्मी स्वतः ही उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, न कि विपरीत दिशा में (बिना बाहरी कार्य के)।
-
द्वितीय नियम “एंट्रॉपी” (Entropy) नामक अवधारणा को भी प्रस्तुत करता है जो किसी तंत्र की अव्यवस्था (disorder) का माप है।
2. मूल कथन (Statements)
(a) क्लॉज़ियस कथन (Clausius Statement):
-
ऊष्मा कभी भी स्वयं (स्वाभाविक रूप से) ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती।
-
यानी, बिना बाहरी कार्य के, बर्फ का टुकड़ा स्वयं कमरे में गर्म नहीं हो सकता।
(b) केल्विन-प्लैंक कथन (Kelvin-Planck Statement):
-
कोई भी ताप इंजिन सम्पूर्णतः उच्च ताप स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे सम्पूर्ण रूप में कार्य में नहीं बदल सकता—कुछ ऊष्मा निम्न ताप सिंक को छोड़नी ही पड़ेगी।
-
अर्थात, 100% ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है।
3. एंट्रॉपी (Entropy)
-
परिभाषा: तंत्र में अव्यवस्था या randomness का माप।
-
प्रत्येक स्वाभाविक प्रक्रिया में संपूर्ण ब्रह्माण्ड की एंट्रॉपी बढ़ती है अथवा स्थिर रहती है (कभी घटती नहीं)।
-
सूत्र:
जहाँ $\Delta S$ = एंट्रॉपी परिवर्तन, $Q_{rev}$ = प्रतिवर्ती (reversible) प्रक्रिया में दी/ली गयी ऊष्मा, $T$ = तापमान (केल्विन में)।
4. द्वितीय नियम के अनुप्रयोग
-
ऊष्मा इंजन: हर इंजन की दक्षता सीमित होती है क्योंकि कुछ ऊष्मा अनिवार्य रूप से निम्न ताप सिंक को जाती है।
-
रेफ्रिजरेटर/हीट पंप: ये तंत्र बाहरी कार्य करके ऊष्मा को ठंडी वस्तु से निकालकर गर्म वस्तु की ओर ले जाते हैं।
-
दैनिक उदाहरण: बर्तन का ठंडा होना, बर्फ का पिघलना—सभी स्वतः ही केवल एक दिशा में घटित होते हैं, विपरीत दिशा में नहीं।
5. मुख्य तथ्य
-
सभी स्वाभाविक ऊष्मीय प्रक्रियाएँ इतनी दिशा में होती हैं कि ब्रह्माण्ड की एंट्रॉपी बढ़े।
-
यह नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन की 100% दक्षता असंभव है—हमेशा कुछ ऊष्मा व्यर्थ होती है।
-
द्वितीय नियम ऊष्मा के प्राकृतिक बहाव, ऊर्जा रूपांतरण और इंजन व मशीनों की सीमाओं को परिभाषित करता है।
6. सारणीबद्ध जानकारी
| विषय | विवरण |
|---|---|
| क्लॉज़ियस कथन | ऊष्मा स्वाभाविक रूप से ठंडे से गर्म वस्तु की ओर नहीं जाती |
| केल्विन–प्लैंक कथन | सम्पूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदलना असंभव |
| एंट्रॉपी | अव्यवस्था का माप, सदैव बढ़ती है या स्थिर रहती है |
| अनुप्रयोग | इंजन, रेफ्रिजरेटर, दैनंदिन जीवन के ऊष्मीय घटनाएँ |
द्वितीय नियम से ही “दिशा” और “अपरिवर्तनीयता” का अर्थ मिलता है—यानी कौन सी प्रक्रियाएँ स्वतः संभव हैं और कौन सी नहीं।

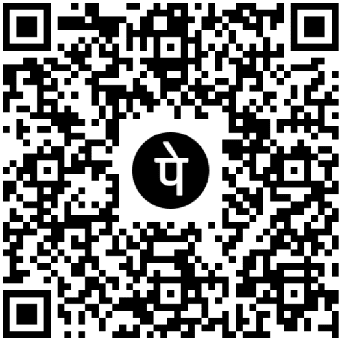




0 Reviews