Read more
भारत में विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी (Science and technology in india)
भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: ऐतिहासिक विकास से वर्तमान तक
1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और योगदान
-
प्राचीन काल: भारत ने गणित (शून्य, दशमलव प्रणाली), ज्योतिष, वैद्यक (आयुर्वेद), धातुशास्त्र (लोहे का अद्वितीय स्तम्भ, लोटल का डॉकयार्ड), और खगोल विज्ञान में वैश्विक योगदान दिया। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, सुष्रुत, चरक जैसे वैज्ञानिकों की खोजों व ग्रंथों ने भारतीय विज्ञान की प्राचीन समृद्धि सिद्ध की।
-
मध्यकालीन काल: इस समयकाल में विज्ञान का विकास जारी रहा; कृषि, रसायनशास्त्र, गणित, चिकित्सा एवं खगोलशास्त्र में नवाचार हुए। इस्लामी और यूरोपीय प्रभाव से नए शैक्षिक संस्थान और तकनीकी विधियाँ आईं।
-
आधुनिक काल (औपनिवेशिक भारत और स्वतंत्रता के बाद): ब्रिटिश शासनकाल में संगठित अनुसन्धान संस्थानों (जैसे – CSIR, DRDO) की स्थापना हुई, आधुनिक शैक्षिक संस्थान (IIT, IISc, NIT) विकसित हुए। स्वतंत्रता के बाद अंतरिक्ष, परमाणु, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी में तेज़ी से प्रगति हुई।
2. संस्थाएं और अकादमियां
-
प्रमुख विज्ञान अकादमियां: इंडियन नेशनल साइंस अकादमी (INSA), इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेज (IAS), नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया (NASI)। ये अकादमियां अनुसन्धान, विज्ञान शिक्षा, और नवाचार को प्रेरित करती हैं।
-
प्रमुख अनुसंधान संस्थाएँ: उपर्युक्त संस्थानों के अलावा, भारत में ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन), BARC (भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र), TIFR, IISER, और अन्य संस्थान विज्ञान व नवाचार के केंद्र हैं।
3. हालिया उपलब्धियां और नीतियां
-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (DST) द्वारा कई इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, शोध सहयोग और इनोवेशन क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत का वैश्विक स्थान लगातार मजबूत हो रहा है — 2025 में भी शोधपत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
-
विज्ञान धारा (Vigyan Dhara) स्कीम (2025) के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा, शोध, नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता दी जा रही है। इससे लाखों युवाओं को रिसर्च व नवाचार के लिए समर्थन मिला है।
4. वर्तमान में भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी (2025 में)
-
टॉप-10 देशों में शामिल: अनुसन्धान एवं विकास (R&D) खर्च, वैज्ञानिक प्रकाशन, और पेटेंट फाइलिंग में भारत अब एशिया में लगभग 10% शेयर रखता है।
-
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति:
-
स्पेस टेक्नोलॉजी: चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान मिशन, उपग्रह प्रक्षेपण आदि।
-
डिजिटल इंडिया मोहिम: 5G, डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा।
-
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कम्प्यूटिंग, सुपरकंप्यूटर: PARAM श्रृंखला के सुपरकंप्यूटर, AI इनोवेशन मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन।
-
नवीकरणीय ऊर्जा व हरित/सतत विकास: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में विश्व नेतृत्व।
-
STEM शिक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप्स: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, और विज्ञान व प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ रहा है।
-
-
सरकारी प्रयास एवं जन सहभागिता: नीति आयोग और राज्य स्तर की STEM परिषदें, स्कूलों व विश्वविद्यालयों में नवाचार लैब्स व इनक्यूबेटर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत STEM शिक्षा का प्रोत्साहन।
5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भविष्य
-
वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स: 2019 में भारत की 52वीं रैंक थी, 2020 में 48वीं — लगातार बेहतर हो रही है।
-
ग्लोबल चैलेंजेस हेतु योगदान: जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट कृषि, हेल्थकेयर, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल वित्त, क्लीन एनर्जी — इन सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।
निष्कर्ष:
भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास निरंतर व बहुआयामी रहा है; प्राचीन उपलब्धियों से लेकर आज के डिजिटल, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी, AI और स्टार्टअप्स युग तक, भारत वैश्विक विज्ञान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है।
भारतीय विज्ञान के विकास के विभिन्न चरण मुख्यतः प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किए जा सकते हैं:
-
प्राचीन काल (लगभग 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक) - इस काल में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने, उसकी धुरी पर घुमने, सूर्य व चंद्र ग्रहण के सही कारण बताए। इसी काल में वैदिक काल के लोग खगोल विज्ञान, गणित, ज्यामिति, और आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रगति कर चुके थे। शून्य की अवधारणा, अंक पद्धति और 'पाई' का मान 3.1416 तक इसी काल में स्थापित हुआ.
-
मध्यकालीन काल (लगभग 200 से 1000 ईस्वी तक) - इस दौरान लल्ल का 'शिष्यधीवृद्धि', संशोधित सूर्यसिद्धांत, नागार्जुन की रसविद्या, सिद्धचिकित्सा, कृषि पाराशर की कृषि विज्ञान संबंधी रचनाएँ हुईं। इस दौर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार हुआ
-
आधुनिक काल (लगभग 18वीं सदी से वर्तमान) - इस काल में British उपनिवेशकालीन भारत में विज्ञान का संगठित विकास और औपचारिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए जैसे 1972 में अंतरिक्ष आयोग, 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण, और 1975 में भारत का पहला उपग्रह 'आर्यभट' प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद चिकित्सा, जैव विज्ञान, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में अनेक विकसित संस्थान व शोध केंद्र बने.
इस प्रकार भारतीय विज्ञान का विकास वैदिक युग से आरंभ होकर खगोल, गणित, चिकित्सा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन योगदानों के साथ मध्यकालीन सुधारों और आधुनिक युग के संस्थागत और तकनीकी विकास के चरणों में हुआ है
भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारशिला प्राचीन काल से ही मजबूत रही है। आधुनिक युग में इसका विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और अधिक गति से हुआ। यहाँ मुख्य बिंदुओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आधारभूत ढांचा प्रस्तुत किया जा रहा है:
1. संस्थागत आधार:
-
स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए अलग-अलग मंत्रालयों एवं विभागों (जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग) की स्थापना की गई।
-
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) जैसी संस्थाएँ वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु आधारभूत ढांचा प्रदान करती हैं।
-
देशभर में विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ, IIT, NIT, IISc, कृषि विश्वविद्यालय, और शोध संस्थान कार्यरत हैं, जो ज्ञान-निर्माण और नवाचार के केंद्र हैं
2. अनुसंधान एवं विकास (R&D):
-
भारत ने R&D में निवेश को प्रमुखता दी है, जिससे बेसिक रिसर्च के साथ-साथ एप्लाइड रिसर्च को बढ़ावा मिला है.
-
परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान (ISRO), जैवप्रौद्योगिकी, फार्मा, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आदि क्षेत्रों में उम्दा शोध और तकनीकी नवाचार हुए हैं।
3. तकनीकी अवसंरचना:
-
देश में विज्ञान पार्क, टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, स्टार्टअप हब, सुपरकंप्यूटिंग केंद्र, टेलीमेडिसिन और टेलीकम नेटवर्क जैसी संरचनाएँ विज्ञान व तकनीक को जन-जन तक पहुंचाती हैं।
-
सुपरसंचार, जल और ऊर्जा क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा मिशन, बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन जैसी योजनाएँ अवसंरचना का हिस्सा हैं.
4. कृषि एवं स्वास्थ्य विज्ञान:
-
हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति में विज्ञान की भूमिका के कारण कृषि उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है.
-
भारतीय विज्ञान का योगदान चिकित्सा, वैक्सीन, और जन स्वास्थ्य में भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
5. शिक्षा एवं मानव संसाधन:
-
देश में विज्ञान शिक्षा को स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रोत्साहित किया गया है।
-
सरकार की नीतियों (जैसे राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1958, टेक्नोलॉजी पॉलिसी 1983 आदि) ने विज्ञान और इंजीनियरिंग की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की है
6. वैश्विक पहचान एवं नवाचार:
-
इनोवेशन रैंकिंग में निरंतर सुधार, स्वदेशी मिसाइल, उपग्रह निर्माण, आईटी और बायोटेक में विश्वस्तरीय उपलब्धियां भारत के वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे को दर्शाती हैं
-
भारत की विज्ञान नीति, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से नवाचार और स्वदेशी तकनीक को समर्थन मिलता है
निष्कर्ष:
भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ढांचा अत्याधुनिक संस्थानों, सुदृढ़ अनुसंधान प्रणाली, वैश्विक नवाचार, और शिक्षा के बेहतर नेटवर्क के साथ निरंतर मजबूत होता जा रहा है। इससे देश के आर्थिक, सामाजिक, रक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं
भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख प्रयोगशालाएँ एवं उनके संबद्ध मंत्रालय/विभाग का संक्षिप्त विवरण :
1. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) — विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
-
CSIR भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसंधान संगठन है, जिसके अंतर्गत 37 विशिष्ट प्रयोगशालाएँ आती हैं। ये प्रयोगशालाएँ विभिन्न औद्योगिक, रसायनिक, औषधि, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में अनुसंधान कर रही हैं।
-
उदाहरण: राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (पुणे), राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (दिल्ली), केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (चेन्नई), राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (जमशेदपुर) आदि।
2. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) — रक्षा मंत्रालय
-
DRDO के तहत लगभग 50 से अधिक अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ हैं, जो रक्षा प्रौद्योगिकी एवं सैन्य उपकरणों के विकास में अग्रणी हैं।
-
उदाहरण: आयुध अनुसन्धान एवं विकास संस्थान (ARDE), रक्षा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट आदि।
3. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) — अंतरिक्ष विभाग
-
ISRO के अंतर्गत भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (अहमदाबाद), अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला (त्रिवेंद्रम), राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (NARL, तिरुपति) जैसी कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ संचालित होती हैं, जो अंतरिक्ष-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य करती हैं।
4. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) — स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
-
ICMR के तहत प्रमुख स्वास्थ्य, जैव-चिकित्सा और वैक्सीन रिसर्च प्रयोगशालाएँ हैं।
-
उदाहरण: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (पुणे) आदि।
5. केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (CDTL) — स्वास्थ्य मंत्रालय
-
यह केंद्र सरकार के अधीन है और औषधि एवं वैक्सीन की गुणवत्ता परीक्षण का कार्य करता है।
6. विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Labs) — गृह मंत्रालय/राज्य सरकारें
-
देशभर में विभिन्न विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ आईएसओ मानकों के अनुसार अपराध अन्वेषण, फोरेंसिक जांच, डिजिटल फॉरेंसिक्स आदि के लिए कार्यरत हैं।
7. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की प्रयोगशालाएँ
-
उदाहरण: भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र आदि।
8. तकनीकी/इंजीनियरिंग एवं कृषि अनुसंधान संस्थान
-
जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), आईआईएससी आदि में आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयोगशालाएँ हैं।
निष्कर्ष:
भारत में मंत्रालय-आधारित प्रयोगशालाओं की एक सशक्त और विविध श्रंखला विकसित है। ये प्रयोगशालाएँ वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, औद्योगिक विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मूलधारा तैयार करती हैं, जिससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को गति मिलती है।
भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के संगठन और विकास के लिए कई मंत्रालय और विभाग कार्यरत हैं। इनके तहत अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी विकास और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए अधीनस्थ संस्थाएँ और योजनाएँ भी संचालित की जाती हैं। यहाँ मुख्य केंद्र सरकार के विभागों की सूची प्रस्तुत है:
1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)
इस मंत्रालय के अंतर्गत तीन प्रमुख विभाग हैं:
-
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology – DST): देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का निर्माण, नवाचार, अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्यक्रमों के समन्वय हेतु मुख्य भूमिका निभाता है।
-
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research – DSIR): औद्योगिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और विविध वैज्ञानिक संस्थाओं (जैसे CSIR) के संचालन के लिए उत्तरदायी।
-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology – DBT): जैवविज्ञान एवं स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण इत्यादि, से जुड़े क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है।
2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences – MoES)
-
मौसम, समुद्र, भूकंप, जलवायु और ध्रुवीय अनुसंधान से संबंधित विषयों में अनुसंधान, निगरानी और नीति निर्माण करता है।
3. अंतरिक्ष विभाग/ISRO (Department of Space)
-
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के संचालन एवं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जिम्मेदारी।
4. परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy – DAE)
-
परमाणु शोध, विद्युत उत्पादन, चिकित्सा एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास एवं प्रयोग।
5. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research – ICMR)
-
स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, जैव-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा।
6. अन्य संबद्ध विभाग/संगठन
-
कृषि अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
-
रक्षा हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
-
विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ (Forensic Science Labs)
7. नीति आयोग (NITI Aayog) का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग
-
समग्र रूप से विज्ञान, तकनीकी एवं नवाचार योजनाओं के मूल्यांकन, नीति-निर्माण तथा राज्य स्तरीय एसटी काउंसिल्स को सहयोग करता है।
निष्कर्ष:
भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्र सरकार अनेक मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन तीनों विभाग (DST, DSIR, DBT) गतिशील और केंद्रीय भूमिका निभाते हैं; अन्य संबंधित मंत्रालय और परिषदें अपने अपने विशेष क्षेत्र में देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों और उन्नति का आधार हैं।

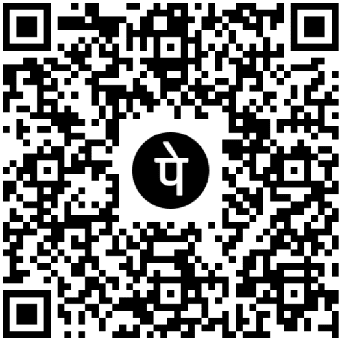




0 Reviews